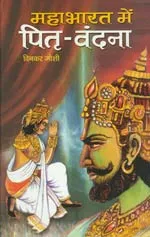|
पौराणिक >> महाभारत में पितृ-वंदना महाभारत में पितृ-वंदनादिनकर जोशी
|
445 पाठक हैं |
||||||
महाभारत के प्रमुख पात्रों के विशिष्ट स्वरूपों का वर्णन....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
महाभारत की बात करें तो कृष्ण और भीम से लेकर अश्वस्थामा और अभिमन्यु तक
के पात्रों की एक पंक्ति-माला रच उठती है। इन पात्रों में भव्यता है तो
उन्हें लेकर प्रश्न भी कम नहीं हैं। प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान लेखक
दिनकर जोशी ने अपने व्यापक और विशिष्ट अध्ययन द्वारा उनका उत्तर देने का
सफल प्रयास किया है और पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, धृतराष्ट्र, कर्ण,
अर्जुन, अश्वस्थामा, शकुनि, द्रुपद एवं श्रीकृष्ण के जीवन के विभिन्न
पक्षों पर सर्वथा अलग तरह से दृष्टि डालते हुए उनके विशिष्ट स्वरूप का
दिग्दर्शन कराया है।
महाभारत का मर्म
साहित्य नामक पदार्थ को पहचानने या समझने के लिए अनेक मापदंड या वर्गीकरण
निर्धारित किए गए हैं। इनमें किसी भी मापदंड या वर्गीकरण से महाभारत नामक
ग्रन्थ को समझने का प्रयत्न करना दर्जी या राजगीर का मेजर-टेप लेकर हिमालय
की ऊँचाई या प्रशांत महासागर की गहराई नापने जैसा हास्यास्पद काम है।
महाभारत को यदि इतिहास कहें तो वह पुराण लगता है और यदि पुराण कहें तो वह
राजवंशियों की कोई कथा लगता है। इसे कथा कहकर इसका मूल्यांकन करने का
प्रयत्न करें तो यह नितांत काव्य लगेगा और यदि काव्य के चश्में से इसे
देखने जाएँ तो यह दर्शनशास्त्र का ग्रन्थ हो, ऐसी प्रतीति होती है।
उपर्युक्त प्रत्येक वर्गीकरण की यथार्थता सिद्ध करने के लिए आवश्यक
शास्त्रीय प्रमाण भी इस ग्रन्थ में से ही प्राप्त किया जा सकता है और
निष्कर्ष का विरोध करने के लिए उतने ही ठोस प्रमाण भी इस ग्रन्थ में से ही
प्राप्त किया जा सकता है और निष्कर्ष का विरोध करने के लिए उतने ही ठोस
प्रमाण भी इस ग्रन्थ में तत्काल उपलब्ध हो सकते हैं। इस प्रकार, महाभारत
का शास्त्रीय स्वरूप प्रथम दृष्टया भ्रामक लगता है; पर इसका सौंदर्य भी
इसकी विशेषता में है।
मानव-रचित कलाकृति को दो बार देखें, चार बार उसका मूल्यांकन करें कि उसकी इतिश्री हो जाती है। यह कृति उसके बाद उस मर्मज्ञ के मन में कोई नया रहस्य प्रकट नहीं करती। कृति की कमनीयता भले ही स्वीकृति मापदंड़ों के आधार पर उच्चतम रहती हो, किन्तु मर्मज्ञ की दृष्टि से एक बार का सूत्र हाथ लग जाए तो उसके बाद उसी मर्मज्ञ के मन में यह कृति नये सौंदर्य प्रकट करने में अपूर्ण ही सिद्ध होती है। प्राकृतिक सौंदर्य में ऐसा नहीं होता। जो सूर्योदय या समुद्री ज्वार की लहरें कल देखी थीं, परसों देखी थीं या उसके पहले भी अनेक बार देखी थीं, उन्हें आनेवाले कल या परसों पुन:-पुन: देखने में उसका वही-का-वही आनंद उसी के उसी तरह प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, सूर्योदय या समुद्र की तरंगे हर बार कोई-न-कोई नया रूप भी प्रकट करती हों, ऐसा लगे बिना नहीं रहता। वही पूर्व दिशा, सूर्य और उसके वही-के-वही रंग या वही-के-वही बादल होते हैं, फिर भी दूसरे या तीसरे दिन अथवा आने वाले हर दिन का सूर्योदय बार-बार नया ही लगता है। ज्वार की लहरों में रहने वाले पानी, वैज्ञानिक पृथक्करण करें तो, उसी के उसी तत्त्व का बना होता है, किंतु बार-बार उसका दर्शन नए-नए सौंदर्य साक्षात्कार कराता है। मानव-रचना पर दैवी रचना का यही तो संकेत है।
महाभारत नामक यह ग्रंथ वैसे तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास नामक एक मनुष्य की ही रचना है, पर उनकी यह रचना मानवीय सीमाओं को लाँघ गई है। विश्व साहित्य का एक भी ग्रन्थ महाभारत की बराबरी करने में समर्थ नहीं है। पाश्चात्य साहित्य के महान् ग्रंथ समझे जाने वाले ‘इलियड’ और ‘ओड़िसी’ इन दोनों की भी महाभारत से तुलना करें तो विस्तार की दृष्टि से अकेले महाभारत ही इनसे आठ गुना अधिक बड़ा है। जीवन की जो व्याप्ति और सर्वांगीण दर्शन महाभारत में है वह तो ‘इलियड’ या ‘ओड़िसी’ के दर्शन की तुलना में आठ सौ गुना है, ऐसा कहने में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। मानव-रचित होने के बावजूद इस ग्रंथ में सूर्योदय या समुद्र के ज्वार जैसी दैवी रचनाओं का जो नित्य नया रूप दिखाई देता है उसके कारण ही उसके विषय में श्रेष्ठ व्यक्तियों ने चिंतन किया है। इसके बावजूद समय-समय पर इसके विषय में लिखा ही जाता रहा है और आनेवाले युगों में भी लिखा जाता रहेगा; क्योंकि इसकी प्रत्येक घटना, इसका प्रत्येक पात्र प्रत्येक वाचन के समय उस सूर्योदय या ज्वार की लहरों की तरह नए रूप, रंग और दर्शन के साथ मर्मज्ञ के समक्ष उपस्थित होते हैं। इसमें कहीं भी गोपन नहीं है, सर्वत्र अभिव्यक्ति और निरी अभिव्यक्ति है।
इसका कारण यह है कि महाभारत समग्र जीवन को सर्वांगीण स्पर्श कराने वाला ग्रंथ है। मानव जीवन रहस्यों से भरपूर है और ये रहस्य पूरी तरह से कभी उद्घाटित नहीं हो सकते। जीवन रहस्य है। उसमें जो दर्शनीय है उसकी तुलना में जो गोपित है वह हिमशिला जैसा है। उसका नौवाँ या दसवाँ भाग ही सतह पर दिखाई देता है और इसीलिए जो गोपित है उसे पाने का प्रयास ही साहित्य का शाश्वत उपादान है। महामनीषी व्यास ने अपने पात्रों या घटनाओं द्वारा जो रहस्य स्फुट किए हैं उससे कहीं अधिक नई समस्याएँ भी पैदा की हैं और स्वयं व्यास ही जब किसी समस्या का सृजन करें तो उसका निराकरण भला दूसरा कौन कर सकता है ! इन समस्याओं को विषय में हम तो मात्र थोड़ा-बहुत अनुमान भर ही कर सकते हैं।
इस महाग्रंथ का आलेखन करने के पीछे उसके सर्जक के मन में क्या उद्देश्य रहा होगा, यह भी तो एक रहस्य ही है। देखने से तो ग्रंथ के आरंभ में ही इसके सर्जक ने ग्रन्थ-रचना के पीछे के अपने उद्देश्य की लंबी सूची अवश्य दी है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुरुवंश की कथा को निमित्त बनाया हो, ऐसा लगता है। पर कुरुवंश के कुछ राजाओं या राजवंशियों के बीच हुए उनके संघर्ष की कथा मात्र ही क्या इसका उद्देश्य हो सकता है ? राजपाट के लिए लड़ते राजवंशियों ने अपना और समाज का समय-समय पर विनाश आमंत्रित किया हो, ऐसी कथाओं से भी कोई भी लेखक या इतिहासकार बखूबी कर सकता है। व्यास जैसे महामानव ऐसे सामान्य काम के लिए इतना बड़ा माहौल रचते होंगे भला ! नहीं, यह तो मात्र घटना है, बाह्य आवरण है। मूलभूत तत्त्व यह कथा नहीं हो सकती।
‘यतो धर्म: ततो जय:’-यह वाक्य महाभारत में बार-बार आता है। कभी-कभी तो यह वाक्य यह आशंका भी पैदा करता है कि महर्षि व्यास ने इस उक्ति के समर्थन में इसे सार्थक करने के लिए ही यह महाग्रंथ रचा होगा। जय मात्र सामर्थ्य से प्राप्त नहीं होती। उद्देश्य और उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाया गया माध्यम अधिक महत्त्व का है। जहाँ अधर्म हो, तो भी उसकी पराजय निश्चित है-और अंतिम विजय तो सत्य की, धर्म की एवं न्याय की ही होती है और यह सत्य, धर्म व न्याय ही कृष्णत्व है। कृष्णत्व कोई नाम नहीं बल्कि सर्वोत्तम की विभावना मात्र है और इसीलिए ‘यतो धर्म: ततो जय:’ की दूसरी पक्ति तत्काल याद आ जाती है- ‘यतो धर्म: ततो जय:’, जहाँ धर्म हो वहीं विजय होती है; किंतु धर्म की पूर्व शर्त कृष्णत्व है ! कृष्ण-रहित धर्म प्लास्टिक के फूल जैसा है।
परन्तु धर्म-विजय की यह बात भी महाभारत के पूर्ववर्ती अनेक ग्रन्थों में अनेक महामानवों ने गा-बजाकर कहाँ नहीं कही है ! फिर इसमें नया क्या है ? उपनिषदों का दर्शन-फिर तो उनकी संख्या अठारह हो या एक सौ आठ-इस धर्म नामक सर्वोपरि तत्व के विषय में भरपूर विचार करता है। जीवन और मृत्यु, उत्पत्ति और संहार-इस चक्र के विषय में उपजे असंख्य प्रश्नों पर विचार करते-करते उपनिषद् के उद्गाताओं ने धर्म-तत्त्व और उसके अंतिम लक्ष्य के विषय में कई गहन बातें महाभारत काल के पूर्व ही कह दी हैं। वेद में स्थूल संघर्षों की कथाएँ हैं, उपनिषदों में उन संघर्षों का समापन है। इस प्रकार, संघर्ष और समापन की बात इसके पूर्व एक या दूसरे प्रकार से विचारी जा चुकी है, चर्चित हो चुकी है।
वेदों की रचना आर्यत्व के उदयकाल को स्पर्श कराती है और इसीलिए उदयकाल में आर्यों ने जिस समृद्ध और सभर जीवन की कामना की है, उसकी प्रति ध्वनि उनमें सुनाई देती है। यह समृद्ध-सभर जीवन उसके सभी पहलुओं के साथ प्राप्त करने के बाद भी कोई अधूरापन तो यथावत् रहा ही है। उसके साक्षात्कार के रूप में जो चिंतन प्रकट हुआ वह उपननिषद्-यात्रा बन गया।
धर्म-विजय ही यदि महाभारत का उद्देश्य रहा होता तो महायुद्ध के अन्त में विजेताओं से व्यास ने करुण क्रंदन न करवाया होता। पांडवों की विजय के साथ ही महाभारत की कथा-यात्रा समाप्त हो जाती; परन्तु ऐसा नहीं हुआ। युधिष्ठिर को जिस सिंहासन की आकांक्षा थी वह उसे प्राप्त हुआ, किन्तु उसकी प्राप्ति का आनंद वह खो चुका था। हजारों स्वजनों की मृत देहों पर उसने करुण विलाप किया है ! पुत्र-विजय की सदैव कामना करने वाले शठ राजा धृतराष्ट्र को लाचार तथा पांडवों का आश्रित बना दिया और विजय का अंतिम उद्घोष करनेवाले कौरव सेनापति अश्वत्थामा को डरावनी परछाईं मात्र बनाकर अमरत्व का अभिशाप उसके ललाट पर लिख दिया गया। करुण विलाप करते समय राजा युधिष्ठिर के मुँह से व्यास ने कहलवाया है-वही जीते जो युद्ध में मारे गए। जय और विजय दोनों अंतत: एक मनोभाव ही हैं। विधि के मन से तो क्या जय, क्या पराजय ! उसके लिए तो संतुलन ही महत्त्व का है। जिन्होंने युद्ध में वीरगति प्राप्त की वे भाग्यशाली थे, क्योंकि स्वजनों-आप्तजनों के स्वयं द्वारा किए संहार के अंत में अब वे व्यथा के आक्रोश से उबर गए थे। जो जीवित बच गए थे और जीवंत रहे थे उनके लिए तो शेष जीवन दहकती भट्ठी जैसा ही रहा !
और यही महाभारत का रहस्य प्रकट हुआ लगता है। महामनीषी व्यास जैसे हाथ उठाकर सतत कह रहे हों- जीवन निरर्थक है ! जय और पराजय इन दोनों का कोई अर्थ नहीं ! भीष्म जैसा महामानव भी शिखंडी के कारण धराशायी हो जाता है और कृष्ण जैसे लोकोत्तर पुरुष भी-पुत्र-पौत्रादि कुत्तों-बिल्लियों की भाँति परस्पर काट-खा रहे हों उस समय-कुछ नहीं कर पाते और हताश अवस्था में एक जंगली पारधी के तीर का भोग बनकर काल के वश हो जाते हैं ! महाकाल ही सर्वोपरि है। मानव-फिर वह कितना ही लोकोत्तर हो- महान् हो, पर महाकाल के समक्ष वह नितांत नगण्य है। महाकाल किसी की गणना नहीं करता। जीवन तो एक अनायास प्राप्त हुई अवस्था है और अंत में तो यह अवस्था व्यर्थ है.....व्यर्थ है.....व्यर्थ ही है।
तत्काल प्रश्न उत्पन्न होता है-व्यर्थता की यह बात व्यास ने किस तरह कही होगी ? ऐसी बात तो भारतीय संस्कृति में चार्वाक कह सकते हैं और पाश्चात्य संस्कृति में एपिक्युरस कह सकते हैं। चार्वाक तो व्यास के भी पुरोगामी थे। तो क्या चार्वाक की इस बात को ही सही ठहराने के लिए व्यास ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया होगा ? शायद.....चार्वाक की सही बात भी गलत तरीके से कही गई थी। संभव है, व्यास ने उस सही बात को सही तरह से कहने की कोशिश की हो ! निस्संदेह भोग व्यर्थ है, उसका तो अंदेशा भी व्यास के पास से प्राप्त नहीं होता; परन्तु वह गंतव्य स्थान है-जीवन की निरर्थकता-केन्द्र स्थान पर रहती है।
महाभारत की बात करें तो तत्काल उसके असंख्य पात्र आँखों के सामने उपस्थित हो जाते हैं। कृष्ण और भीष्म से लेकर ठेठ अश्वत्थामा और अभिमन्यु तक के पात्रों की एक पंक्ति माला रच उठती है। इन पात्रों में भव्यता है तो उन्हें लेकर प्रश्न भी कम नहीं हैं चांडाल-चौकड़ी का मुख्य पात्र समझे जानेवाले दुर्योधन महायुद्ध के भीषण क्षण में सात्य से किकहता है, ‘‘हे मित्र ! हम दोनों परम सखा होने के बावजूद एक-दूसरे के घातकी शत्रु बन गए हैं। धिक्कार है हमारे क्षात्र-धर्म को ! धिक्कार है हमारे अहंकार और मोह को !’’ ऐसी अति दुष्कर प्रामाणिकता भी प्रकट करता है। दूसरी ओर सदैव धर्मराज के रूप में प्रख्यात महात्मा युधिष्ठिर, ‘‘द्यूत खेलकर मैं कौरवों का राज्य ठीन लेना चाहता था।’’
ऐसी आघातजनक स्वीकारोक्ति करते हैं। अकेले अपने बल पर समग्र आर्यावर्त के राजाओं को जिन्होंने परास्त किया था, ऐसे प्रचंड पराक्रमी भीष्म ‘‘समर्थ व्यक्ति जो कहे वही धर्म है।’’ ऐसी बात कहकर कुलवधू द्रौपदी को निर्वस्त्र किए जाने के दृश्य को असहाय होकर देखते रहे। इतना ही नहीं, युद्ध के आरंभ में आशीर्वाद माँगने आए युधिष्ठिर से स्वयं को नपुंसक और दुर्योधन के धन के पालित होने की दीनतापूर्ण बात कहते हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है ! धर्म के उत्तुंग खिखर समान स्वयं कृष्ण द्रौपदी के पाचों पुत्रों को गहरी नींद में ही अश्वत्थामा मार डालने वाला है, यह जानते हुए भी उनकी रक्षा नहीं कर सके, यह घटना कैसे समझाई जा सकती है ? ऐसे-ऐसे अनेक प्रश्न महाभारत के प्रत्येक प्रमुख पात्र के आस-पास जुड़े हुए हैं।
मानव-रचित कलाकृति को दो बार देखें, चार बार उसका मूल्यांकन करें कि उसकी इतिश्री हो जाती है। यह कृति उसके बाद उस मर्मज्ञ के मन में कोई नया रहस्य प्रकट नहीं करती। कृति की कमनीयता भले ही स्वीकृति मापदंड़ों के आधार पर उच्चतम रहती हो, किन्तु मर्मज्ञ की दृष्टि से एक बार का सूत्र हाथ लग जाए तो उसके बाद उसी मर्मज्ञ के मन में यह कृति नये सौंदर्य प्रकट करने में अपूर्ण ही सिद्ध होती है। प्राकृतिक सौंदर्य में ऐसा नहीं होता। जो सूर्योदय या समुद्री ज्वार की लहरें कल देखी थीं, परसों देखी थीं या उसके पहले भी अनेक बार देखी थीं, उन्हें आनेवाले कल या परसों पुन:-पुन: देखने में उसका वही-का-वही आनंद उसी के उसी तरह प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, सूर्योदय या समुद्र की तरंगे हर बार कोई-न-कोई नया रूप भी प्रकट करती हों, ऐसा लगे बिना नहीं रहता। वही पूर्व दिशा, सूर्य और उसके वही-के-वही रंग या वही-के-वही बादल होते हैं, फिर भी दूसरे या तीसरे दिन अथवा आने वाले हर दिन का सूर्योदय बार-बार नया ही लगता है। ज्वार की लहरों में रहने वाले पानी, वैज्ञानिक पृथक्करण करें तो, उसी के उसी तत्त्व का बना होता है, किंतु बार-बार उसका दर्शन नए-नए सौंदर्य साक्षात्कार कराता है। मानव-रचना पर दैवी रचना का यही तो संकेत है।
महाभारत नामक यह ग्रंथ वैसे तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास नामक एक मनुष्य की ही रचना है, पर उनकी यह रचना मानवीय सीमाओं को लाँघ गई है। विश्व साहित्य का एक भी ग्रन्थ महाभारत की बराबरी करने में समर्थ नहीं है। पाश्चात्य साहित्य के महान् ग्रंथ समझे जाने वाले ‘इलियड’ और ‘ओड़िसी’ इन दोनों की भी महाभारत से तुलना करें तो विस्तार की दृष्टि से अकेले महाभारत ही इनसे आठ गुना अधिक बड़ा है। जीवन की जो व्याप्ति और सर्वांगीण दर्शन महाभारत में है वह तो ‘इलियड’ या ‘ओड़िसी’ के दर्शन की तुलना में आठ सौ गुना है, ऐसा कहने में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है। मानव-रचित होने के बावजूद इस ग्रंथ में सूर्योदय या समुद्र के ज्वार जैसी दैवी रचनाओं का जो नित्य नया रूप दिखाई देता है उसके कारण ही उसके विषय में श्रेष्ठ व्यक्तियों ने चिंतन किया है। इसके बावजूद समय-समय पर इसके विषय में लिखा ही जाता रहा है और आनेवाले युगों में भी लिखा जाता रहेगा; क्योंकि इसकी प्रत्येक घटना, इसका प्रत्येक पात्र प्रत्येक वाचन के समय उस सूर्योदय या ज्वार की लहरों की तरह नए रूप, रंग और दर्शन के साथ मर्मज्ञ के समक्ष उपस्थित होते हैं। इसमें कहीं भी गोपन नहीं है, सर्वत्र अभिव्यक्ति और निरी अभिव्यक्ति है।
इसका कारण यह है कि महाभारत समग्र जीवन को सर्वांगीण स्पर्श कराने वाला ग्रंथ है। मानव जीवन रहस्यों से भरपूर है और ये रहस्य पूरी तरह से कभी उद्घाटित नहीं हो सकते। जीवन रहस्य है। उसमें जो दर्शनीय है उसकी तुलना में जो गोपित है वह हिमशिला जैसा है। उसका नौवाँ या दसवाँ भाग ही सतह पर दिखाई देता है और इसीलिए जो गोपित है उसे पाने का प्रयास ही साहित्य का शाश्वत उपादान है। महामनीषी व्यास ने अपने पात्रों या घटनाओं द्वारा जो रहस्य स्फुट किए हैं उससे कहीं अधिक नई समस्याएँ भी पैदा की हैं और स्वयं व्यास ही जब किसी समस्या का सृजन करें तो उसका निराकरण भला दूसरा कौन कर सकता है ! इन समस्याओं को विषय में हम तो मात्र थोड़ा-बहुत अनुमान भर ही कर सकते हैं।
इस महाग्रंथ का आलेखन करने के पीछे उसके सर्जक के मन में क्या उद्देश्य रहा होगा, यह भी तो एक रहस्य ही है। देखने से तो ग्रंथ के आरंभ में ही इसके सर्जक ने ग्रन्थ-रचना के पीछे के अपने उद्देश्य की लंबी सूची अवश्य दी है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुरुवंश की कथा को निमित्त बनाया हो, ऐसा लगता है। पर कुरुवंश के कुछ राजाओं या राजवंशियों के बीच हुए उनके संघर्ष की कथा मात्र ही क्या इसका उद्देश्य हो सकता है ? राजपाट के लिए लड़ते राजवंशियों ने अपना और समाज का समय-समय पर विनाश आमंत्रित किया हो, ऐसी कथाओं से भी कोई भी लेखक या इतिहासकार बखूबी कर सकता है। व्यास जैसे महामानव ऐसे सामान्य काम के लिए इतना बड़ा माहौल रचते होंगे भला ! नहीं, यह तो मात्र घटना है, बाह्य आवरण है। मूलभूत तत्त्व यह कथा नहीं हो सकती।
‘यतो धर्म: ततो जय:’-यह वाक्य महाभारत में बार-बार आता है। कभी-कभी तो यह वाक्य यह आशंका भी पैदा करता है कि महर्षि व्यास ने इस उक्ति के समर्थन में इसे सार्थक करने के लिए ही यह महाग्रंथ रचा होगा। जय मात्र सामर्थ्य से प्राप्त नहीं होती। उद्देश्य और उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाया गया माध्यम अधिक महत्त्व का है। जहाँ अधर्म हो, तो भी उसकी पराजय निश्चित है-और अंतिम विजय तो सत्य की, धर्म की एवं न्याय की ही होती है और यह सत्य, धर्म व न्याय ही कृष्णत्व है। कृष्णत्व कोई नाम नहीं बल्कि सर्वोत्तम की विभावना मात्र है और इसीलिए ‘यतो धर्म: ततो जय:’ की दूसरी पक्ति तत्काल याद आ जाती है- ‘यतो धर्म: ततो जय:’, जहाँ धर्म हो वहीं विजय होती है; किंतु धर्म की पूर्व शर्त कृष्णत्व है ! कृष्ण-रहित धर्म प्लास्टिक के फूल जैसा है।
परन्तु धर्म-विजय की यह बात भी महाभारत के पूर्ववर्ती अनेक ग्रन्थों में अनेक महामानवों ने गा-बजाकर कहाँ नहीं कही है ! फिर इसमें नया क्या है ? उपनिषदों का दर्शन-फिर तो उनकी संख्या अठारह हो या एक सौ आठ-इस धर्म नामक सर्वोपरि तत्व के विषय में भरपूर विचार करता है। जीवन और मृत्यु, उत्पत्ति और संहार-इस चक्र के विषय में उपजे असंख्य प्रश्नों पर विचार करते-करते उपनिषद् के उद्गाताओं ने धर्म-तत्त्व और उसके अंतिम लक्ष्य के विषय में कई गहन बातें महाभारत काल के पूर्व ही कह दी हैं। वेद में स्थूल संघर्षों की कथाएँ हैं, उपनिषदों में उन संघर्षों का समापन है। इस प्रकार, संघर्ष और समापन की बात इसके पूर्व एक या दूसरे प्रकार से विचारी जा चुकी है, चर्चित हो चुकी है।
वेदों की रचना आर्यत्व के उदयकाल को स्पर्श कराती है और इसीलिए उदयकाल में आर्यों ने जिस समृद्ध और सभर जीवन की कामना की है, उसकी प्रति ध्वनि उनमें सुनाई देती है। यह समृद्ध-सभर जीवन उसके सभी पहलुओं के साथ प्राप्त करने के बाद भी कोई अधूरापन तो यथावत् रहा ही है। उसके साक्षात्कार के रूप में जो चिंतन प्रकट हुआ वह उपननिषद्-यात्रा बन गया।
धर्म-विजय ही यदि महाभारत का उद्देश्य रहा होता तो महायुद्ध के अन्त में विजेताओं से व्यास ने करुण क्रंदन न करवाया होता। पांडवों की विजय के साथ ही महाभारत की कथा-यात्रा समाप्त हो जाती; परन्तु ऐसा नहीं हुआ। युधिष्ठिर को जिस सिंहासन की आकांक्षा थी वह उसे प्राप्त हुआ, किन्तु उसकी प्राप्ति का आनंद वह खो चुका था। हजारों स्वजनों की मृत देहों पर उसने करुण विलाप किया है ! पुत्र-विजय की सदैव कामना करने वाले शठ राजा धृतराष्ट्र को लाचार तथा पांडवों का आश्रित बना दिया और विजय का अंतिम उद्घोष करनेवाले कौरव सेनापति अश्वत्थामा को डरावनी परछाईं मात्र बनाकर अमरत्व का अभिशाप उसके ललाट पर लिख दिया गया। करुण विलाप करते समय राजा युधिष्ठिर के मुँह से व्यास ने कहलवाया है-वही जीते जो युद्ध में मारे गए। जय और विजय दोनों अंतत: एक मनोभाव ही हैं। विधि के मन से तो क्या जय, क्या पराजय ! उसके लिए तो संतुलन ही महत्त्व का है। जिन्होंने युद्ध में वीरगति प्राप्त की वे भाग्यशाली थे, क्योंकि स्वजनों-आप्तजनों के स्वयं द्वारा किए संहार के अंत में अब वे व्यथा के आक्रोश से उबर गए थे। जो जीवित बच गए थे और जीवंत रहे थे उनके लिए तो शेष जीवन दहकती भट्ठी जैसा ही रहा !
और यही महाभारत का रहस्य प्रकट हुआ लगता है। महामनीषी व्यास जैसे हाथ उठाकर सतत कह रहे हों- जीवन निरर्थक है ! जय और पराजय इन दोनों का कोई अर्थ नहीं ! भीष्म जैसा महामानव भी शिखंडी के कारण धराशायी हो जाता है और कृष्ण जैसे लोकोत्तर पुरुष भी-पुत्र-पौत्रादि कुत्तों-बिल्लियों की भाँति परस्पर काट-खा रहे हों उस समय-कुछ नहीं कर पाते और हताश अवस्था में एक जंगली पारधी के तीर का भोग बनकर काल के वश हो जाते हैं ! महाकाल ही सर्वोपरि है। मानव-फिर वह कितना ही लोकोत्तर हो- महान् हो, पर महाकाल के समक्ष वह नितांत नगण्य है। महाकाल किसी की गणना नहीं करता। जीवन तो एक अनायास प्राप्त हुई अवस्था है और अंत में तो यह अवस्था व्यर्थ है.....व्यर्थ है.....व्यर्थ ही है।
तत्काल प्रश्न उत्पन्न होता है-व्यर्थता की यह बात व्यास ने किस तरह कही होगी ? ऐसी बात तो भारतीय संस्कृति में चार्वाक कह सकते हैं और पाश्चात्य संस्कृति में एपिक्युरस कह सकते हैं। चार्वाक तो व्यास के भी पुरोगामी थे। तो क्या चार्वाक की इस बात को ही सही ठहराने के लिए व्यास ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया होगा ? शायद.....चार्वाक की सही बात भी गलत तरीके से कही गई थी। संभव है, व्यास ने उस सही बात को सही तरह से कहने की कोशिश की हो ! निस्संदेह भोग व्यर्थ है, उसका तो अंदेशा भी व्यास के पास से प्राप्त नहीं होता; परन्तु वह गंतव्य स्थान है-जीवन की निरर्थकता-केन्द्र स्थान पर रहती है।
महाभारत की बात करें तो तत्काल उसके असंख्य पात्र आँखों के सामने उपस्थित हो जाते हैं। कृष्ण और भीष्म से लेकर ठेठ अश्वत्थामा और अभिमन्यु तक के पात्रों की एक पंक्ति माला रच उठती है। इन पात्रों में भव्यता है तो उन्हें लेकर प्रश्न भी कम नहीं हैं चांडाल-चौकड़ी का मुख्य पात्र समझे जानेवाले दुर्योधन महायुद्ध के भीषण क्षण में सात्य से किकहता है, ‘‘हे मित्र ! हम दोनों परम सखा होने के बावजूद एक-दूसरे के घातकी शत्रु बन गए हैं। धिक्कार है हमारे क्षात्र-धर्म को ! धिक्कार है हमारे अहंकार और मोह को !’’ ऐसी अति दुष्कर प्रामाणिकता भी प्रकट करता है। दूसरी ओर सदैव धर्मराज के रूप में प्रख्यात महात्मा युधिष्ठिर, ‘‘द्यूत खेलकर मैं कौरवों का राज्य ठीन लेना चाहता था।’’
ऐसी आघातजनक स्वीकारोक्ति करते हैं। अकेले अपने बल पर समग्र आर्यावर्त के राजाओं को जिन्होंने परास्त किया था, ऐसे प्रचंड पराक्रमी भीष्म ‘‘समर्थ व्यक्ति जो कहे वही धर्म है।’’ ऐसी बात कहकर कुलवधू द्रौपदी को निर्वस्त्र किए जाने के दृश्य को असहाय होकर देखते रहे। इतना ही नहीं, युद्ध के आरंभ में आशीर्वाद माँगने आए युधिष्ठिर से स्वयं को नपुंसक और दुर्योधन के धन के पालित होने की दीनतापूर्ण बात कहते हैं। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है ! धर्म के उत्तुंग खिखर समान स्वयं कृष्ण द्रौपदी के पाचों पुत्रों को गहरी नींद में ही अश्वत्थामा मार डालने वाला है, यह जानते हुए भी उनकी रक्षा नहीं कर सके, यह घटना कैसे समझाई जा सकती है ? ऐसे-ऐसे अनेक प्रश्न महाभारत के प्रत्येक प्रमुख पात्र के आस-पास जुड़े हुए हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book